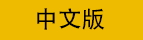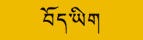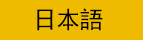थेगछेन छोलिंग, धर्मशाला, भारत, ७ जून २०१६ - परम पावन दलाई लामा के निवास स्थान के समक्ष मुख्य तिब्बती मन्दिर चुगलगखंग में ७००० लोगों का एक मिला जुला जनमानस उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनमें हिमालय क्षेत्र, अधिकतर लाहौल-स्पीति से ४५०, यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी (वाई बी एस), उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के ३५० सदस्य, तमिलनाडु से ३० और भारत के अन्य भागों से ४०० लोग शामिल थे। उनके साथ ७८ देशों से १७०० विदेशी, १५०० तिब्बती भिक्षु और भिक्षुणियाँ और तिब्बती जनता के ३५०० लोग भी सम्मिलित हुए।
प्रवचनों की इस श्रृंखला का अनुरोध तथा आयोजन नालंदा शिक्षा, भारतीय मित्रों के एक समूह, जिनके सदस्यों ने सभी प्रामाणिक जीवंत बौद्ध परम्पराओं के प्रख्यात शिक्षकों के साथ अध्ययन किया है, के सदस्यों द्वारा हुआ है। उन्होंने श्रवण, चिंतन तथा मनन के अभ्यास को जीवित रखने में रुचि दिखाई है। उन्होंने इसके पूर्व परम पावन के प्रवचनों का चार अवसरों पर आयोजन किया है, २०१२, २०१३ में धर्मशाला, २०१४ में मुंबई तथा २०१५ में संकिसा। उनके अनुरोध पर परम पावन दो महत्वपूर्ण ग्रंथों पर शिक्षा दे चुके हैं, कमलशील के 'भावनाक्रम' और शांतिदेव के 'बोधिसत्वचर्यावतार'। नालंदा शिक्षा ने किसी भी विशिष्ट स्कूल या वंश के पूर्वाग्रह के बिना, पूरे बौद्धधर्म और इसकी प्रामाणिक परम्पराओं और आचार्यों के लिए कार्य करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

|
परम पावन द्वारा सिंहासन पर स्थान ग्रहण करते ही पालि परम्परा के भारतीय भिक्षुओं ने पालि में जयमंगल अट्ठ गाथा का पाठ किया। तत्पश्चात नालंदा शिक्षा की ओर से, वीर सिंह ने भारतीय आतिथ्य परम्परा के अनुसार समर्पण प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट की, जिसमें पीने हेतु जल, पैर धोने के लिए जल, पुष्प, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य तथा शब्द शामिल थे। इन वस्तुओं को एक ट्रे पर रखकर क्रम से परम पावन के समक्ष लाया गया। परम पावन ने टिप्पणी की:
"हम इस प्रकार के समर्पण तांत्रिक अनुष्ठानों में भी करते हैं। इस तरह के समर्पण हमें स्मरण कराते हैं कि बौद्ध धर्म एक भारतीय परम्परा है। और आज भारत में दोनों तरह के लोग हैं, एक जिनके लिए बौद्ध धर्म उनके लम्बे समय से चली आ रही विरासत है और दूसरे जिन्होंने इसे नए सिरे अपनाया है, जिनमें डॉ आंबेडकर के अनुयायी हैं।
"बुद्ध शाक्यमुनि का जीवन भारत में बीता और उन्होंने जो शिक्षा दी उसका संरक्षण बाद में तक्षशिला, विक्रमशील और नालंदा जैसे महान शिक्षण संस्थानों में किया गया। जब तिब्बती सम्राट ठिसोंग देचेन ने ८वीं शताब्दी ईस्वी में शांतरक्षित को तिब्बत आने के लिए आमंत्रित किया, तो वे हिम प्रदेश में नालंदा परम्परा लेकर आए। तिब्बती १००० वर्षों से अधिक इस परंपरा के संरक्षक रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से आप भारतीय हमारे शिक्षक थे, पर उसके बाद से, हम शिष्यों ने परम्परा को जीवित रखा है। अतः अब इसे आपके साथ साझा करते हुए मुझे विशेष तरह की अनुभूति होती है।"
परम पावन ने उल्लेख किया कि ऐसा कुछ जो भारत, आर्यों की भूमि को अनूठा रूप देता है वह यह कि है कि १००० वर्षों से विश्व के सभी प्रमुख धर्म यहाँ पोषित हुए हैं। सांख्य, जैन और बौद्ध परम्पराएँ जैसी स्वदेशी परम्पराएँ हैं जिनके साथ पारसी, यहूदी, ईसाई और इस्लाम जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि यही वह स्थान है जहाँ हम इन सभी परम्पराओं को पारस्परिक सम्मान के सहित एक साथ रहते हुए पाते हैं और इस रूप में यह दूसरों के लिए पालन करने हेतु एक प्रारूप है। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म सहित भारत की मननशील परम्पराएँ, चित्त के कार्य की प्राचीन समझ रखती हैं, जो आज भी प्रासंगिक तथा रुचि का विषय बना हुआ है।
परम पावन ने बल देते हुए कहा कि जबकि कुछ धार्मिक परम्पराएँ आस्तिक हैं और एक सृजनकर्ता ईश्वर के अस्तित्व पर बल देती हैं, अन्य गैर- आस्तिक हैं और इसके स्थान पर कार्य कारण, हेतु और प्रभाव पर बल देती हैं। पर फिर भी, वे सभी प्रेम व करुणा के महत्व का संदेश और सहिष्णुता, संतोष तथा आत्म अनुशासन द्वारा इन गुणों की रक्षा करने की आवश्यकता के महत्व का एक ही संदेश देते हैं। ये ऐसी परम्पराएँ हैं जिनसे अतीत में लाभ हुआ है, इस समय लाभदायक हैं, और भविष्य में ये लाभकारी रहेगी। वे विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों पर ज़ोर दे सकते हैं पर सभी प्रेम और करुणा के अभ्यास को पोषित करते हैं। इसी कारण उनके बीच अंतर्धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

|
परम पावन ने आगे कहा, "बुद्ध की अनूठी देशना चार आर्य सत्य, कार्य कारण के नियम पर आधारित है और अंततः स्थायी सुख की ओर ले जाती है। उन्होंने न तो एक सृजनकर्ता ईश्वर पर बल दिया और न ही एक स्वाभाव सत्ता रखने वाले आत्म पर। जो लोग उनके बाद आए जैसे नागार्जुन और असंग और उनके अनुयायियों ने संस्कृत में व्याख्यात्मक ग्रंथ लिखे। समय के साथ बुद्ध के वचनों का भोट भाषा में अनुवाद से कांग्यूर के १०० खंड बने और उन ग्रंथों के अनुवाद से तेंग्यूर के २२० खंड बने।
"इन खंडों के आधार पर पांच प्रमुख विज्ञानः बौद्ध सिद्धांत और अभ्यास का आंतरिक विज्ञान, भाषा, तर्क, भैषज और कला और शिल्प और व्याकरण इत्यादि के पाँच गौण विज्ञान बनाए गए। मेरे शिक्षक ने मुझे संस्कृत व्याकरण पढ़ाया, पर अब वह ज्ञान शून्यता में विलीन हो गया है।"
एक लघु अंतराल के दौरान परम पावन ने श्रोताओं को प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया और प्रथम मृत्यु से संबंधित था। परम पावन ने कहा कि चार आर्य सत्य के प्रथम व्याख्यान के दौरान अनित्यता संदर्भित की गई थी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म अनित्यता है जिसका संदर्भ क्षणिक परिवर्तन से है, तथा स्थूल अनित्यता जो उस समय प्रकट होती है जब कि एक पुष्प खिलता है, मुरझाता है और मर जाता है। उन्होंने कहा कि अपने आध्यात्मिक अभ्यास के एक अंग के रूप में प्रत्येक दिन मृत्यु के तथ्य पर चिन्तन करना उपयोगी है। उन्होंने कहा कि तांत्रिक अभ्यास का एक नियमित अंग नित्य प्रति मृत्यु की प्रक्रिया, विघटन के आठ चरण की कल्पना है जो वास्तविक मृत्यु के एक तरह से तैयारी के रूप हो सकती है। उन्होंने समाप्त करते हुए कहा:
"मृत्यु जीवन का एक अंग है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।"
एक अन्य प्रश्नकर्ता उनसे भिक्षु के चीवरों के विषय में जानना चाहते थे और परम पावन ने समझाया कि आम तौर पर उन्हें नीले, लाल या पीले रंग का होना चाहिए, परन्तु काला अथवा सफेद नहीं। तिब्बत जैसे ठंडी जलवायु के लिए लाल रंग अधिक व्यावहारिक है, जबकि थाईलैंड, श्रीलंका और बर्मा में भिक्षु भगवे रंग का वस्त्र पहनते हैं। रंग जो भी हो, चीवरों को पैबन्द अथवा कपड़ों के टुकड़ों से बना होना चाहिए। भिक्षुओं को एक जोड़े चीवर की अनुमति है जिसे वे अपना कह सकते हैं। यदि उनके पास इससे अधिक हो तो उन्हें समुदाय का माना जाना चाहिए। इसी प्रकार कुल १३ वस्तुएँ हैं जो एक भिक्षु के पास हो सकती हैं, और उन्हें आशीर्वचित करने की एक प्रक्रिया है।
हिमालयी क्षेत्र और नालंदा परम्परा के बीच संबंधों के संबंध में, परम पावन ने कहा:
"मुझे महत्वपूर्ण शिक्षाएँ विश्व के उस भाग के आचार्यों से प्राप्त हुईं। खुनु लामा रिनपोछे से मुझे 'बोधिसत्वचर्यावतार' का संचरण और शिक्षा प्राप्त हुई और गेशे रिगजिन तेनपा से मैंने जे चोंखापा की 'सुवर्ण माला' सुनी। इन दिनों हमारे महाविहारीय संस्थानों में उस क्षेत्र से ४०० भिक्षु अध्ययन कर रहे हैं। उनमें से कई शिक्षक बनेंगे।
"वसुबंधु ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा के दो पहलू हैं: आगम और अधिगम। मात्र अध्ययन और अभ्यास से हम उन्हें संरक्षित कर पाएँगे। आगम के संबंध में जिसमें व्याख्यान देना और सुनना शामिल है और अधिगम के संबंध में जिसमें तीन अधिशिक्षाओं का प्रशिक्षण है। हिमालयी क्षेत्र को जितना बन पड़े अध्ययन और अभ्यास करना चाहिए। इसमें केवल भिक्षु ही नहीं अपितु भिक्षुणियाँ और उपासक भी शामिल हैं।
"जब हम कहते हैं 'मैं त्रिरत्न में शरण लेता हूँ' तो हमें समझने की आवश्यकता है कि त्रिरत्न क्या हैं, उनके कारण क्या हैं। और हमारी समझ को तर्क का समर्थन मिलना चाहिए।"
शांतिदेव के 'बोधिसत्वचर्यावतार' की ओर लौटते हुए परम पावन ने वह बात दोहराई जो खुनु लामा रिनपोछे ने उनसे कही थी कि ८वीं शती में जब से शांतिदेव ने इस ग्रंथ की रचना की थी तब से बोधिचित्तोत्पाद के लिए इससे अधिक महान ग्रंथ की रचना नहीं हुई है। उन्होंने कहा:
"शांतिदेव के स्रोत नागार्जुन की 'रत्नावली' और 'बोधिचित्त पर भाष्य’, जो कि गुह्यसमाज तंत्र के एक अध्याय पर टिप्पणी है, थे। बोधिचित्तोत्पाद के लिए नागार्जुन के स्रोत में 'अवतंशक सूत्र' और प्रज्ञा पारमिता सूत्र शामिल हैं।
"बुद्ध संबुद्धि प्राप्त करने के पश्चात यह सोचकर मौन रहे कि उन्होंने जो पाया था - शून्यता की गहन अंतर्दृष्टि, उसे कोई और नहीं समझ पाएगा। अंततः उन्होंने सार्वजनिक रूप से चार आर्य सत्यों उनके १६ आकारों, ३७ बोधिपाक्षिक धर्मों की शिक्षा दी। शून्यता का एक और अधिक संपूर्ण विवरण उन्होंने गृद्ध कूट पर एक विशिष्ट समूह को दिया। तो तीन धर्म चक्र प्रवर्तनों में प्रथम का संबंध चार आर्य सत्य से था, दूसरे का प्रज्ञा पारमिता से और तीसरे का बुद्ध प्रकृति तथा चित्त के स्वरूप से था।"
परम पावन ने कहा कि वह पुस्तक में से कुछ न पढ़ेंगे परन्तु इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि इसमें उपाय तथा प्रज्ञा और सत्य द्वय को लेकर क्या कहा गया है। उन्होंने कहा कि वस्तुएँ जिस रूप से दिखाई देती हैं, उस रूप में अस्तित्व नहीं रखती और इस संबंध में हमारी भ्रांति ही है जो हमारी नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि हम दूसरों के लिए चिंता का विकास करते हुए आत्म-पोषण की हमारी प्रवृत्ति का प्रतिकार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि 'बोधिचर्यावतार' के नवे अध्याय का संबंध शून्यता से है पर उसे ठीक से समझने के लिए अन्य पुस्तकों के पठन और अध्ययन की आवश्यकता है।
प्रवचन कल जारी रहेंगे।