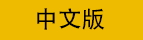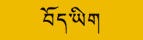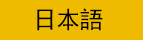ओसाका, जापान, १२ मई २०१६ - कई दिनों के बादल और वर्षा के पश्चात आज ओसाका की आँखें खिड़कियों से छनती प्रातः उज्ज्वल सूर्य के प्रकाश और ऊपर उज्ज्वल नीले आसमान से खुली। जैसे ही परम पावन दलाई लामा होटल से होते हुए ओसाका इंटरनेशनल कॉनफ्रेंस सेंटर की ओर पैदल निकले तो प्रकाश की किरणों से भवनों के चहुँ ओर के वृक्षों की ताजी पत्तियाँ भर गईं।
एक बार जब वे बैठ गए तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया "आज मैं आपको पथक्रम परम्परा के विषय में बताना चाहता हूँ," "८वीं सदी में शांतरक्षित सम्राट ठिसोंग देचेन के निमंत्रण पर तिब्बत आए। वह अपने समय के नालंदा विश्वविद्यालय के एक अग्रणी विद्वान थे और उन्होंने तिब्बत में विशुद्ध नालंदा परम्परा की स्थापना की। ठि रलपाचेन के शासनकाल के पश्चात तिब्बत राजनीतिक रूप से खंडित हो गया।
"देश के पश्चिम में, गुगे का साम्राज्य ञारी था जिसकी राजधानी थोलिंग थी। शांतरक्षित और गुरु पद्मसंभव द्वारा स्थापित परम्पराएँ, जिनका ह्रास हो गया था, की पुनर्स्थापना हेतु राजा भारत से बौद्ध शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहता था। एक स्थानीय अनुवादक, रिनछेन ज़ंगपो पहले से ही इस क्षेत्र में सक्रिय थे जब राजा ने दीपांकर अतीश को विक्रमशिला विश्वविद्यालय से तिब्बत आने के लिए राजी किया।"
परम पावन ने समझाया कि राजा ने अतीश से एक ऐसे शिक्षण की रचना करने का अनुरोध किया जो विशेष रूप से तिब्बतियों के लिए उपयुक्त हो और उसके उत्तर में उन्होंने 'बोधिपथप्रदीप' की रचना की। यह इस ग्रंथ को अन्य भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों से इस रूप में अलग करता है कि यह एक व्यक्ति के आध्यात्मिक अभ्यास - पथ के क्रमों के सम्पूर्ण मार्ग को प्रस्तुत करता है। उन्होंने इन मार्गों के अभ्यासियों को तीन प्रकार की क्षमताओँ के संदर्भ में वर्णित किया। हीन क्षमता वाले उच्चतर पुनर्जन्म का उद्देश्य रखते हैं। मध्यम श्रेणी के क्षमता वाले लोग भवचक्र के दुःख से मुक्ति की खोज में रहते हैं तथा उच्च श्रेणी के क्षमता वाले लोग प्रबुद्धता की आकांक्षा रखते हुए करुणा तथा बोधिचित्त का विकास करते हैं।

|
परवर्ती तिब्बती लेखकों के लिए ‘पथ के क्रम’ एक प्रारूप बन गया। ञिङमा आचार्य लोंगछेनपा ने अपने ‘चित्त विश्रान्त’ में उसका अनुपालन किया, काग्यू दगपो ल्हजे अपने 'मुक्तिरत्नालंकार' में ऐसा किया, जो बुद्ध प्रकृति की एक व्याख्या के साथ प्रारंभ होता है। सक्या आचार्यों ने अपने 'मार्ग और फल’ ग्रंथों में इस रूप का पालन किया। और अंततः कदम्प परम्परा के संस्थापक जे चोंखापा ने अपने पथक्रम के कई ग्रथों में 'बोधिपथप्रदीप' पर टिप्पणी तथा भाष्य लिखे। उन्होंने छह कदम्प ग्रंथों का भी संदर्भ दिया जिसमें 'बोधिसत्चर्यावतार' एक था।
परम पावन ने समझाया कि 'अभिसमयालंकार' के अनुसार सत्य द्वय और चार आर्य सत्य के आधार पर ही लोग त्रिरत्न की शरण में जाते हैं। उन्होंने टिप्पणी की, कि जब वे मुक्ति की संभावना और यह क्या है, को समझते हैं, तो वे प्रेरित होंगे। यह उसकी तुलना में बहुत अधिक प्रभावी है, जब उन्हें नरक की संभावना से भयभीत किया जाता है, यदि वे निर्देशों का पालन न करते। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने इस रूप में शिक्षा दी जिसमें कि लोग सहजता का अनुभव कर सकें तथा जोड़ा कि यह बौद्ध धर्म की प्रबल पृष्ठभूमि है जो इसे विज्ञान के साथ संवाद करने में तैयार करती है।
'बोधिसत्वचर्यावतार' की ओर मुड़ते हुए परम पावन ने आठवाँ अध्याय से पढ़ना प्रारंभ किया, जो क्षांति से संबंधित है और एक सीधी सलाह से प्रारंभ हैः
क्षांति रखते हुए मुझे वीर्य का विकास करना चाहिए,
क्योंकि बोधिचित्त उनमें ही निवास करता है
जो स्वयं प्रयास करते हैं
उन्होंने जो हम करना चाहते हैं उसमें आत्मविश्वास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि कैसे क्लेशों के संबंध में इसमें जागरूकता और सतर्कता के योग की आवश्यकता है। यदि आप कुछ करने से पहले क्लेशों को जन्म लेने की अनुमति देते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, इसके पूर्व कि वे विस्फोटित हों आपको उन्हें पकड़ने और उनसे निपटना पड़ेगा।

|
ध्यान के अध्याय की ओर जाते हुए उन्होंने व्याख्यायित किया कि मुख्य विषय एकाग्र चित्त का विकास है, एक ऐसा अभ्यास जो अन्य अबौद्ध भारतीय परम्पराओं द्वारा भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि 'शमथ' स्थिरता के बारे में है, पर आवश्यक नहीं कि शारीरिक रूप से स्थिर हो पर चित्त धारणात्मक विचारों से पूरी तरह रिक्त। ग्रंथ चर्चा करता है कि किस तरह शमथ का विकास करे, चित्त को केन्द्रित करने के लिए किस तरह वस्तु का चयन करे और यह किस प्रकार शैथिल्य अथवा उत्तेजना से बाधक हो सकता है। परम पावन ने सलाह दी कि बौद्ध प्रायः ध्यान केन्द्रित करने के लिए बुद्ध की छवि का चयन करते हैं, पर कुछ परम्पराएँ मात्र स्पष्टता और चित्त की सजगता को वस्तु के रूप में चयन करते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जहाँ शांतिदेव इच्छा और स्त्रियों के लिए वासना के आकर्षण का किस तरह प्रतिकार किया जाए, की बात कर रहे थे, उस समय वे भिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे। वे जो कहते हैं वह समान तौर पर स्रियों के लिए पुरुषों को लेकर लागू होता है।
परात्मसमपरिवर्तन के संबंध में शांतिदेव का विशिष्ट स्पष्टीकरण इस चिंतन के साथ प्रारंभ होता है:
सर्वप्रथम मुझे एक प्रयास करना होगा
आत्म और अन्य की समता पर भावना के लिए,
मुझे अपने ही समान सभी सत्वों की रक्षा करनी चाहिए
क्योंकि हम सभी सुख (चाहने) में
और दुःख को (न चाहने) में समान हैं
और आगे कहते हैं :
जो भी शीघ्रता से सुरक्षा चाहते हैं
अपने और अन्य सत्वों के लिए
उसे उस पावन रहस्य का अभ्यास करना चाहिए:
परात्मसमपरिवर्तन
परम पावन ने टिप्पणी की कि इसके तंत्र के अभ्यास जो गुह्य है, के साथ संबंध के कारण अन्य के लिए आदान प्रदान को एक रहस्य के रूप में संदर्भित किया जाता है, पर साथ ही इसलिए भी कि यह कुछ ऐसा है जिसे हर कोई नहीं कर सकता। अभ्यास का सार संक्षेप में निम्नलिखित श्लोक में दिया गया है:
इस संसार में जो भी सुख है
वह दूसरों को सुखी देखने की इच्छा से आता है,
और इस संसार जो भी दुःख है
सब स्वयं के सुख की इच्छा से आता है।
मध्याह्न में भोजन से लौटने के बाद, परम पावन ने सलाह दी कि जब ध्यान के विषय में निर्देश की बात आती है तो वह एक पुस्तक सुझाते हैं, भावना क्रम, जो भारतीय आचार्य और शांतरक्षित के शिष्य कमलशील द्वारा तिब्बत में रचित है।
'बोधिसत्वचर्यावतार' के नवें अध्याय का प्रारंभ करते हुए जो प्रज्ञा से संबंधित है उन्होंने टिप्पणी की:
बुद्ध पाप को जल से धोते नहीं,
न ही जगत के दुःखों को अपने हाथों से हटाते हैं;
न ही अपने अधिगम को दूसरों में स्थान्तरण करते हैं;
वे धर्मता सत्य देशना से सत्वों को मुक्त कराते हैं।
यह अध्याय सत्य द्वय को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बौद्ध परम्पराओं के विचारों, विशेष रूप से चित्तमात्र के साथ मध्यमक के विरोधाभासों को प्रस्तुत करता है। यह सबसे पहले पुद्गलों (व्यक्तियों) की नैरात्म्यता और उसके बाद धर्मों की नैरात्म्यता की खोज करता है। यह निष्कर्ष निकालता है:
अतः यह जीवन निरर्थक रूप से शीघ्र बीतता है
और वास्तविकता की जांच करने के अवसर की खोज बहुत कठिन है।
ऐसी स्थिति में इसके प्रतिलोम के लिए क्या उपाय है
वास्तविक अस्तित्व की ग्राह्यता के अनादि आदत पर?
अतः पुनः (एक मानव जीवन का) पाना कठिन होगा ,
तथा बुद्धों की उपस्थिति पाना अत्यंत कठिन है।
व्याकुल करने वाली धारणाओं के इस प्रवाह को त्यागना कठिन है।
हा , सत्वों के दुःख की निरंतरता तो बनी रहेगी !
और इस तरह (वास्तविक अस्तित्व का) संदर्भ
सम्मान पूर्वक पुण्य संभार करते हुए,
जब अन्यों का संदर्भ देते हुए, मैं शून्यता को प्रकट करने में सक्षम होऊँगा
जो पीड़ित और दु:खी हैं?

|
जैसे मध्याह्न का समय समाप्त होने को आया, परम पावन ने टिप्पणी की कि उन्होंने ग्रंथ के हर श्लोक को नहीं पढ़ा था, परन्तु शांतिदेव की रचना की भावना और अर्थ के सम्प्रेषण का प्रयास किया था। जो चर्चा हमने की है उस पर चिन्तन करें। यह एक कहानी की तरह नहीं है, इसे पढ़ें और इस पर सोचें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी और आपकी व्याकुल करने वाली भावनाओं में कमी होने लगेगी।
"कल मैं पहले उपासक के नियम प्रदान करूँगा, जिसके विषय में अतीश ने कहा कि वे एक अच्छा आधार बनते हैं जिसके बाद बोधिसत्व संवर तथा मंजुश्री अनुज्ञा दूँगा। हम 'हृदय सूत्र' का पाठ करेंगे। चूँकि हम जापान में हैं हम पहले इसका पाठ जापानी में और बाद में मंदारिन में करेंगे। आप में से जो लोग रूसी, मंगोलियाई, कोरियाई, तिब्बती या अंग्रेजी बोलते हैं वे अपनी भाषा में स्वयं पाठ कर सकते हैं।"
जैसे ही परम पावन सभागार से निकले एक बार पुनः २७०० श्रोताओं ने मैत्रीपूर्ण उत्साह के साथ तालियाँ बजाई।