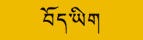मैं आधुनिक समय में धर्म की प्रासंगिकता पर बात करना चाहूँगा। स्वभावतया प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं की भावना होती है और उसके साथ जानने वाली बातों की दुःख, प्रसन्नता या तटस्थ भावनाएँ अनुभूत होती हैं। ये सब तथ्य हैं जिनके जाँच की कोई आवश्यकता नहीं है। जानवरों में भी यह है। स्वभाव से हम सबको सुख अच्छा लगता है तथा दुःख अच्छा नहीं लगता। इसको प्रमाणित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर, हम सभी सुखी जीवन प्राप्त करने और पीड़ा पर काबू पाने के अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं।

अब, पीड़ा तथा आनन्द के दो वर्ग हैं। एक शारीरिक ऐन्द्रिक अनुभव से और एक अन्य चैतसिक स्तर से जुड़ा हुआ है। ऐन्द्रिक स्तर स्तनधारियों की सभी प्रजातियों के लिए सामान्य है जिनकी पाँच इंद्रियाँ हैं। जहाँ तक मानसिक स्तर की बात है, यह कुछ जानवरों में होता है। परन्तु चूँकि इंसानों में अत्यधिक विकसित बुद्धि है, अतः उनके पास दीर्घकाल की स्मृति और भविष्य को लेकर विचार होते हैं। यह जानवरों से अधिक है। अतः मानवों में मानसिक आनन्द और संतुष्टि या पीड़ा - आशा, भय है। अतः शारीरिक सुख और दुख और मानसिक सुख और दुख अलग बातें हैं। हम शारीरिक पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं, परन्तु चैतसिक सुख के साथ और अन्य समय हमारा शारीरिक स्तर ठीक है, पर हमारा मानसिक स्तर चिंता और असंतोष से भरा होता है।
शारीरिक स्तर भौतिक सुविधाओं से संबंधित है - भोजन, कपड़े, आश्रय, अच्छे दृश्य ध्वनि, गंध, स्वाद, शारीरिक अनुभूति, सामग्री सुविधाएँ। कुछ लोग बहुत धनवान हैं। उनके पास प्रतिष्ठा, शिक्षा, सम्मान, कई मित्र होते हैं। पर फिर भी, व्यक्तियों के रूप में, वे बहुत दुखी व्यक्ति हैं। यह इसलिए है कि भौतिक सुविधाएँ मानसिक संतुष्टि या आराम लाने में असफल रहती हैं। कोई तनावभरी, चिंता, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, घृणा, मोह - ये मानसिक दुख लाते हैं। अतः शारीरिक तथा भौतिक हित की सीमाएँ हैं। यदि हम आंतरिक स्तर की उपेक्षा करें तो हो सकता है कि जीवन सुखी न हो। सम्पन्न समाजों में भौतिक आराम मिलता है, पर वे सुनिश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि वहाँ लोगों के चित्त सुखी, शांतिपूर्ण, आरामदायी हैं। अतः चित्त की शांति लाने के लिए हमें एक उपाय की आवश्यकता है।
साधारणतया, धर्म मानसिक शांति और संतोष लाने का एक साधन है, कुछ आस्था लिए हुए मानसिक शान्ति। कई लोग सहमत हैं कि चित्त की शांति लाने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष उपाय होना चाहिए, पर मैं उसकी चर्चा अपने सार्वजनिक व्याख्यान में करूँगा। पर यदि हम आस्था के आधार पर चित्त की शांति लाने की बात करें तो धर्म के दो वर्ग हैं - बिना दर्शन के आस्था और दर्शन के साथ आस्था।
प्राचीन काल में लोग आशा और शान्ति लाने के लिए आस्था का उपयोग करते थे जब उनके समक्ष संकट से भरी परिस्थितियाँ आती थीं - हमारे नियंत्रण से परे समस्याएँ, नैराश्य। ऐसी परिस्थितियों में, आस्था कुछ आशा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, रात में जानवरों का खतरा है तो अंधकार से किंचित भय। प्रकाश होने पर हम और अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। प्रकाश का स्रोत सूर्य है, अतः सूर्य कुछ पवित्र है और इसलिए कुछ लोगों ने सूर्य की आराधना की। जब हमें ठंड लगती है तो अग्नि आरामदायक होती है तो कुछ ने अग्नि को अच्छे रूप में माना। अग्नि कभी कभी बिजली से आती है, जो रहस्यमय है और इसलिए अग्नि और बिजली दोनों पवित्र हैं। ये आदिम आस्थाएँ हैं, जिनका कोई दर्शन नहीं है।
एक अन्य वर्ग में संभवतः प्राचीन मिस्र का समाज सम्मिलित है। मुझे उसके बारे में नहीं पता। मिस्र की सभ्यता छह या सात हजार वर्ष प्राचीन है और उसमें आस्था का स्थान था। जब मैं काहिरा के विश्वविद्यालयों में से एक में था, तो मैंने रुचि जताई कि यदि मेरे पास अधिक समय हो तो मैं वहाँ अध्ययन करना चाहूँगा और इस प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में अधिक सीखना चाहूँगा पर दुर्भाग्य से मेरे पास समय नहीं है। पर जो भी हो, धर्म के एक और वर्ग में भारत की सिंधु घाटी सभ्यता और चीनी सभ्यता शामिल है। वे एक विचारधारा के साथ और अधिक परिष्कृत धर्म थे। संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरों की तुलना में अधिक था। भारत में, तीन या चार हजार वर्ष पूर्व पहले से ही आस्था थी जिसका एक निश्चित दर्शन था। इस तरह, धर्म का एक और वर्ग आस्था है जिसके साथ कुछ दार्शनिक अवधारणाएँ हैं।
इस दूसरे वर्ग में, सामान्य प्रश्न हैं। एक यहूदी मित्र ने उन्हें अच्छी तरह से प्रस्तुत किया: "मैं" क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये मुख्य प्रश्न हैं। इनके उत्तर के दो वर्ग हैं: ईश्वरवादी तथा अनीश्वरवादी।
भारत में, तीन हज़ार वर्ष पूर्व लोगों ने "मैं " क्या है?, आत्म क्या है?, इसका उत्तर ढूँढने का प्रयास किया था। सामान्य अनुभव के अनुसार, शरीर जब युवा होता है तो उसका रूप तथा आकार वृद्धावस्था की तुलना में अलग होता है। चित्त भी क्षणों में अलग होता है। पर हममें "मैं" को लेकर एक सहज भावना है - जब "मैं" युवा था, जब "मैं" बूढ़ा था। अतः, शरीर और चित्त का एक स्वामी होना चाहिए। स्वामी एक स्वतंत्र और नित्य हो, अपरिवर्तनशील हो, जबकि शरीर और चित्त में परिवर्तन होता है। तो, भारत में, एक आत्म, एक आत्मा, एक "आत्मन" - यह विचार आता है। जब शरीर काम के योग्य नहीं रह जाता तो वहाँ आत्मा बनी रहती है। "मैं" क्या है?, का यही उत्तर है।
फिर, आत्मा कहाँ से आती है? इसका कोई आदि है अथवा नहीं? कोई आदि न हो इसे स्वीकार करना कठिन है और इसलिए प्रारंभ होना चाहिए, जैसे कि इस शरीर का प्रारंभ है। और इसलिए ईश्वर आत्मा निर्मित करते हैं। और जहाँ तक अंत की बात है तो हम ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं अथवा अंततः हम ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। मध्य पूर्वी धर्म - प्रारंभिक यहूदी, ईसाई, और शायद मिस्र के - बाद के जीवन में विश्वास करते हैं। परन्तु यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के लिए, परम सत्य ईश्वर है, निर्माता। वही सब का स्रोत है। उस ईश्वर में असीम शक्ति और असीम करुणा और प्रज्ञा होनी चाहिए। प्रत्येक धर्म असीम करुणा पर बल देता है, जैसे अल्लाह। और ईश्वर हमारे अनुभव से परे है, परम सत्य। यह ईश्वरीय धर्म है।
फिर, लगभग तीन हज़ार वर्ष पूर्व हमें भारत में सांख्य दर्शन मिलता ह। और इसके अंदर दो वर्ग समक्ष आए: एक ईश्वर पर विश्वास करता है और एक कहता है कोई ईश्वर नहीं। इसके बजाय, बाद का वर्ग प्रकृति तथा २५ तत्वों की बात करता है। अतः उनके लिए, प्रकृति स्थायी और निर्माता है। तो बुद्ध से पूर्व, पहले से ही अनीश्वरवादी विचार थे।
फिर, लगभग २६०० वर्ष पूर्व बुद्ध और जैन के संस्थापक महावीर आए। उनमें से कोई भी ईश्वर का उल्लेख नहीं करता, पर इसके स्थान पर केवल कार्य कारण पर बल दिया। इस तरह सांख्य का एक वर्ग तथा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अनीश्वरवादी धर्म हैं।
अनीश्वरवादी धर्मों में बौद्ध धर्म का कहना है कि सब कुछ स्व हेतुओं व परिस्थितियों से आता है, और इसलिए कार्य कारण की प्रकृति ही परिवर्तन की है। वस्तुएँ कभी अचल रूप में नहीं होतीं। अतः चूँकि आत्म या "मैं" का आधार शरीर और चित्त है, जो स्पष्ट रूप से हर क्षण परिवर्तनशील हैं और चूँकि "मैं" उन पर निर्भर करता है, तो "मैं" की प्रकृति समान होना चाहिए। यह अपरिवर्तनशील और स्थायी नहीं हो सकता। यदि आधार परिवर्तित होता है तो उस पर नामित में भी परिवर्तन होना चाहिए। अतः कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील आत्मा नहीं है - "अनात्मन"। यह अनूठी बौद्ध अवधारणा है - सब कुछ अन्योन्याश्रित और संबंधित। इसलिए, तीन अनीश्वरवादी धर्मों में, यद्यपि अन्य दो कारणों को स्वीकार करते हैं, पर फिर भी वे एक स्थायी, अपरिवर्तनशील आत्म पर बल देते हैं।
तो, आस्था के साथ दर्शन रखने वाले धर्मों में, कई अलग-अलग परम्पराएँ हैं। इन सभी के दो पक्ष हैं - दर्शन और अवधारणाएँ और अभ्यास भी। दर्शन और अवधारणाओं के संदर्भ में बहुत बड़ा अंतर है, पर अभ्यास समान है - प्रेम, करुणा, क्षमा, सहिष्णुता, आत्म-अनुशासन। विभिन्न दर्शन और अवधारणाएँ लोगों में प्रेम, करुणा, क्षमा इत्यादि के व्यवहार लाने की इच्छा और दृढ़ विश्वास के मात्र उपाय हैं। अतः, इन सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य और उद्देश्य है - प्रेम, करुणा, इत्यादि लाना।
यह बौद्ध धर्म में स्पष्ट है। बुद्ध ने विभिन्न अवधारणाओं की देशना दी, प्रायः विरोधाभासी प्रतीत होने वाले। कुछ सूत्र कहते हैं कि स्कंध - काय व चित्त एक भार के समान है जो आत्म वहन करती है। भार और जो उसका वहन कर रहे है वह एक नहीं हो सकते, और इसलिए आत्म को पृथक होना चाहिए और उसका अस्तित्व होना चाहिए। एक अन्य सूत्र कहता है कि कर्म का अस्तित्व है, पर कोई व्यक्ति नहीं जो कार्य करता है, कोई ठोस अस्तित्व रखने वाला आत्म नहीं। अन्य सूत्र कहते हैं कि है कि कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। मात्र चित्त है और अन्य वस्तुएँ मात्र चित्त का विषय हैं। एक चित्त का अस्तित्व है, वह यथार्थ में अस्तित्व रखता है। पर फिर अन्य सूत्र कहते हैं कि न तो चित्त का और न ही उसके विषय वास्तव में अस्तित्व रखते हैं - किसी का भी वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, जैसा कि प्रज्ञा -पारमिता सूत्र, हृदय सूत्र में आता है उदाहरण के लिए, "न चक्षु, न श्रोत्र, न नासिका, न जिह्वा, न काय, न चित्त।" ये सभी विरोधाभासी हैं, पर वे सब एक ही स्रोत से आते हैं, शाक्यमुनि बुद्ध।
बुद्ध ने यह सब अपने भ्रम से नहीं सिखाया। और न ही उन्होंने उन्हें जानबूझकर अपने शिष्यों में भ्रम फैलाने के लिए दिया। उन्होंने इस तरह की देशना क्यों दी? बुद्ध ने इस बात के प्रति सम्मान दिखाया कि व्यक्ति विभिन्न हैं और उन्होंने यह सब उनकी सहायता के लिए देशित किया। उन्होंने देखा कि ये सब आवश्यक थे।
तीन हजार वर्ष पूर्व संभवतः दस या एक सौ करोड़ लोग थे। अब सात अरब से अधिक हैं। तो, इन सभी लोगों में निश्चित रूप से विभिन्न स्वभाव हैं। यह हम एक ही माता पिता के बच्चों में भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी उनके चित्त और भावनाएँ अलग-अलग होती हैं। अतः मनुष्यों के बीच, विभिन्न स्वभाव, जीवन के विभिन्न तरीके, चिन्तन के अलग-अलग भेद हैं। ये अंतर भी पर्यावरण, भूगोल और जलवायु द्वारा अनुकूलित होते हैं। उदाहरणार्थ अरब गर्म और शुष्क है। भारत में मानसून की वर्षा है अतः यह अलग है और लोगों की अलग-अलग जीवन शैली है। संभवतः आदिम काल में, लोग हर स्थान पर अधिक समानता रखते थे। पर अब, इन विभिन्नताओं के कारण, विभिन्न दृष्टिकोणों का होना महत्वपूर्ण है। पर इन विभिन्न दर्शनों तथा अवधारणाओं से वास्तव में कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण उन सभी का उद्देश्य और लक्ष्य है और यह समान है: दूसरों के प्रति दृष्टिकोण में दयालु और करुणाशील व्यक्ति होना।
तब कुछ लोगों के लिए, एक सृजनकर्ता की अवधारणा, ईश्वर, बहुत सहायक है। मैंने एक बार एक वयोवृद्ध ईसाई भिक्षु से पूछा कि ईसाई धर्म विगत जीवनों में क्यों विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा, "क्योंकि यह जीवन ही ईश्वर द्वारा निर्मित है।" इस तरह की सोच से ईश्वर के साथ अंतरंगता अनुभव होती है। यह शरीर हमारी माँ के गर्भ से आता है और इसलिए हम अपनी माँ से निकटता और आराम का अनुभव करते हैं। इसलिए, ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है। हम ईश्वर से आते हैं और यह हमें ईश्वर के साथ निकटता की भावना प्रदान करता है। जितनी निकटता का अनुभव होगा उतना ही प्रबल ईश्वर की सलाह का पालन करने का उद्देश्य होगा। अतः, ईश्वरवादी दृष्टिकोण बहुत शक्तिशाली है और कई लोगों के लिए अनीश्वरवादी दृष्टिकोण की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी है।
अपनी स्वयं की धार्मिक परम्परा बनाए रखना अधिक उचित है। मंगोलिया में, मिशनरी ईसाई धर्म में मतांतरण करने हेतु लोगों को १५ डॉलर देते हैं। तो कुछ लोग उनके पास बार बार हर वर्ष धर्मांतरण करने जाते हैं और हर बार १५ डॉलर इकट्ठा करते हैं। मैं इन मिशनरियों को सलाह देता हूँ कि वे हस्तक्षेप न करें और लोगों को पारम्परिक बौद्ध बने रहने दें। यह उसी तरह है जब मैं पाश्चात्य लोगों को अपने धर्मों में बने रहने के लिए कहता हूँ।
सबसे अच्छा अधिक जानकारी रखना है। यह सम्मान विकसित करने में सहायता करता है। इसलिए यदि आप ईसाई हैं तो अपनी ईसाई परम्परा को बनाए रखें, पर अन्य परम्पराओं की समझ और ज्ञान प्राप्त करें। जहाँ तक उपायों का संबंध है, सभी में समान अभ्यास सिखाया जाता है - प्रेम, करुणा, सहिष्णुता। चूँकि अभ्यासों को आम रूप से साझा किया जाता है तो बौद्ध धर्म के कुछ उपाय अपनाना ठीक है। पर बौद्ध अवधारणा कि कुछ भी पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं है - यह केवल बौद्धों के लिए है। दूसरों को इसकी शिक्षा उपयोगी नहीं है। एक ईसाई पादरी ने मुझसे शून्यता के विषय में पूछा और मैंने उनसे कहा कि यह उनके लिए अच्छा नहीं है। यदि मैं पूरी तरह से अन्योन्याश्रितता सिखाता हूँ तो यह उनके ईश्वर पर प्रबल आस्था को हानि पहुँचा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वे शून्यता के बारे में हो रही बात न सुनें।
संक्षेप में, चूँकि सभी प्रमुख परम्पराओं में एक ही अभ्यास है, मात्र अलग-अलग उपाय और विभिन्न दर्शन हैं, पर एक ही उद्देश्य है, यह पारस्परिक सम्मान का आधार है। तो, अपनी स्वयं की परम्परा बनाए रखें। पर यदि मेरे व्याख्यान से कुछ बौद्ध उपाय आपको उपयोगी लगें तो उन्हें काम में लाएँ। यदि वे उपयोगी नहीं हैं तो उन्हें छोड़ दें।
परम पावन १४वें दलाई लामा
studybuddhism.com सौजन्य से